भारत की स्वतंत्रता और उसके नए संविधान के लागू होने के साथ ही देश की प्रगति की नींव रखी गई। स्वतंत्रता के तुरंत बाद हमारे देश का नेतृत्व आधुनिक भारत के निर्माता पं. जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया। नेहरू जी का यह यह मानना था कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का एक ही रास्ता है- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को विकास से जोड़ा जाए। नेहरू जी ने मुख्यत: दो क्षेत्रों मे अपना ध्यान केन्द्रित किया – परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का विकास और इसके माध्यम से अंतरिक्ष विज्ञान का विकास और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अंतर्गत देश में एक के बाद एक कई वैज्ञानिक संस्थाओं और प्रयोगशालाओं की स्थापना। भारत मे नाभिकीय ऊर्जा के व्यवहार्य और दूरदर्शी कार्यक्रम की स्थापना होमी जहाँगीर भाभा और नेहरू जी के संयुक्त दृष्टिकोणों के परिणामस्वरूप हुई। आइए, भारत को नाभिकीय युग मे प्रवेश दिलाने मे भाभा की भूमिका के बारे मे चर्चा करते हैं।
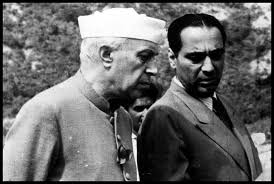
भाभा के साथ पं. नेहरू
होमी भाभा का जन्म 30 अक्तूबर, 1909 को मुंबई मे एक सम्पन्न पारसी परिवार मे हुआ था। स्कूली शिक्षा मे शानदार अकादमिक प्रदर्शन के बाद भाभा ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए कैंब्रिज विश्वविद्यालय मे प्रवेश लिया। भौतिकी मे उनकी व्यापक दिलचस्पी थी, इसलिए उन्होने नाभिकीय भौतिकी को अपना अनुसंधान क्षेत्र चुना। कैंब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी करने के बाद वहीं उन्हें प्राध्यापक के रूप मे नियुक्ति मिली। भाभा ने भौतिकी के चोटी के वैज्ञानिकों, रदरफोर्ड, डिराक, चैडविक, बोर, आइंस्टाइन, पौली आदि के साथ कार्य किया। भाभा का शोधकार्य मुख्यत: कॉस्मिक किरणों पर केंद्रित था। कॉस्मिक किरणें अत्यधिक ऊर्जा वाले वे कण होते हैं जो बाहरी अंतरिक्ष मे पैदा होते हैं और छिटक कर पृथ्वी पर आ जाते हैं। भाभा ने वर्ष 1937 मे वाल्टर हाइटलर के साथ मिलकर कॉस्मिक किरणों पर एक सैद्धांतिक शोधपत्र प्रकाशित करवाया। उनके कॉस्मिक किरणों पर किये गए शोध कार्य को वैश्विक स्तर पर व्यापक मान्यता प्राप्त हुई। तब तक भाभा एक प्रतिष्ठित भौतिक विज्ञानी बन चुके थे।
द्वितीय विश्व युद्ध की भारत को देन
यह एक संयोग ही कहा जा सकता है कि वर्ष 1939 मे भाभा कैंब्रिज से कुछ दिनों की छुट्टी लेकर भारत आए। और इसी बीच यूरोप मे अचानक द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। इसलिए उन्होने विश्व युद्ध के ख़त्म होने तक भारत मे ही रहने का निर्णय किया। और उन्होने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइन्स, बैंगलोर मे चंद्रशेखर वेंकट रामन के आमंत्रण पर रीडर के पद पर नियुक्ति प्राप्त की। इससे भाभा के जीवन में एक बड़ा मोड़ा तो आया ही साथ मे भारत के वैज्ञानिक विकास को भी एक नई दिशा मिली।
प्रारम्भ मे भाभा का अनुसंधान कार्य कॉस्मिक किरणों पर ही केंद्रित था, मगर नाभिकीय भौतिकी के क्षेत्र मे विकास को देखते हुए भाभा को यह विश्वास हो गया कि इस क्षेत्र के अनुसन्धानों से भारत निकट भविष्य में लाभ उठा सकेगा। वर्ष 1944 में भाभा ने टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष दोराब जी टाटा को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होने नाभिकीय भौतिकी के क्षेत्र में मौलिक अनुसंधान हेतु एक संस्थान के निर्माण का प्रस्ताव रखा तथा नाभिकीय विद्युत की उपयोगिता पर प्रकाश डाला। टाटा ट्रस्ट के अनुदान से वर्ष 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामैंटल रिसर्च (टीआईएफ़आर) की डॉ. होमी भाभा के नेतृत्व में स्थापना हुई। टीआईएफ़आर ने भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को संगठित करने के लिए आधारभूत ढांचा उपलब्ध करवाया।
दो महान विभूतियों के बीच अद्भुत बौद्धिक संबंध
भारत मे परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम संबंधी वैज्ञानिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का श्रेय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू और होमी भाभा की दूरदर्शिता को जाता है। भाभा की प्रतिभा के नेहरू जी कायल थे तथा दोनों के बीच काफी मधुर संबंध थे। वर्ष 1948 में भाभा की अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई। यह भाभा की दूरदृष्टि ही थी कि नाभिकीय विखंडन की खोज के बाद जब सारी दुनिया नाभिकीय ऊर्जा के विध्वंसनात्मक रूप परमाणु बम के निर्माण मे लगी हुई थी तब भाभा ने भारत की ऊर्जा जरूरतों को ध्यान मे रखते हुए विद्युत उत्पादन के लिए परमाणु शक्ति के उपयोग की पहल की। भाभा के नेतृत्व में भारत में प्राथमिक रूप से विद्युत शक्ति पैदा करने तथा कृषि, उद्योग, चिकित्सा, खाद्य उत्पादन और अन्य क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए नाभिकीय अनुप्रयोगों के विकास की रूपरेखा तैयार की गई। इस दौरान भाभा को नेहरू जी की निरंतर सहायता और प्रोत्साहन मिलती रही, जिससे भारत दुनिया भर के उन मुट्ठी भर देशों में शामिल हो सका जिनको सम्पूर्ण नाभिकीय चक्र पर स्वदेशी क्षमता हासिल था।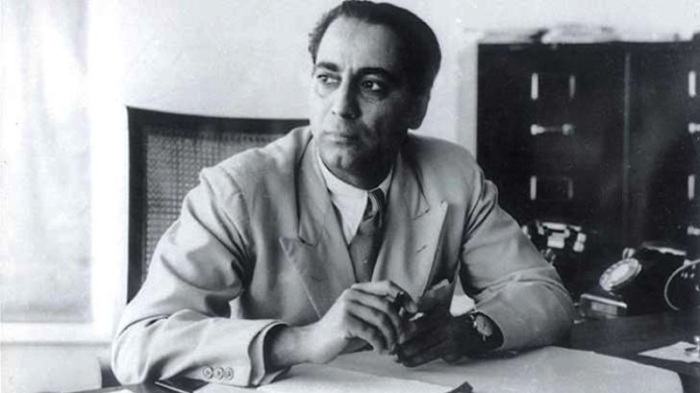
त्रिस्तरीय नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम
डॉ. भाभा ने देश में उपलब्ध यूरेनियम और थोरियम के विपुल भंडारों को देखते हुए परमाणु विद्युत उत्पादन की तीन स्तरीय योजना बनाई थी, जिसमें क्रमश: यूरेनियम आधारित नाभिकीय रिएक्टर स्थापित करना, प्लूटोनियम को ईंधन के रूप मे उपयोग करना तथा थोरियम चक्र पर आधारित रिएक्टरों की स्थापना करना शामिल था। इस त्रिस्तरीय योजना का दो हिस्सा भारत पूरा कर चुका है। इस प्रकार भाभा ने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में भारत को स्वावलंबी बनाकर उन लोगों के दाँतो तले ऊंगली दबा दिया जो परमाणु ऊर्जा के विध्वंसनात्मक उपयोग के पक्षधर थे।
परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के पक्षधर
परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग से संबंधित भाभा का विजन सम्पूर्ण मानवता के लिए युगांतरकारी सिद्ध हुआ। उन्होने यह बता दिया कि परमाणु का उपयोग सार्वभौमिक हित और कल्याण के लिए करते हैं, तो इसमें असीम संभावनाएं छिपी हुई है। वर्ष 1955 में भारत के प्रथम नाभिकीय रिएक्टर ‘अप्सरा’ की स्थापना परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग की दिशा में पहला सफल कदम था। इसके बाद भाभा के नेतृत्व में साइरस, जरलीना आदि रिएक्टर अस्तित्व में आए। हालांकि डॉ. भाभा शांतिपूर्ण कार्यों के लिए परमाणु ऊर्जा के उपयोग के पक्षधर रहे, लेकिन 1962 के भारत-चीन युद्ध मे भारत की हार ने उन्हें अपनी सोच बदलने को विवश कर दिया। इसके बाद वे कहने लगे कि ‘शक्ति का न होना हमारे लिए सबसे महंगी बात है’। अक्तूबर 1965 में डॉ. भाभा ने ऑल इंडिया रेडियों से घोषणा कि अगर उन्हें मौका मिले तो भारत 18 महीनों में परमाणु बम बनाकर दिखा सकता है। उनके इस वक्तव्य ने सारी दुनिया में सनसनी पैदा कर दी। हालांकि इसके बाद भी वे विकास कार्यों में परमाणु ऊर्जा के उपयोग की वकालत करते रहे तथा ‘शक्ति संतुलन’ हेतु भारत को परमाणु शक्ति सम्पन्न बनना आवश्यक बताया।
विमान दुर्घटना और असामयिक मृत्यु
24 जनवरी, 1966 को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग की बैठक मे भाग लेने के लिए विएना जाते हुए एक विमान दुर्घटना में मात्र 57 वर्ष की आयु में डॉ. भाभा का निधन हो गया। इस प्रकार भारत ने एक उत्कृष्ट वैज्ञानिक, प्रशासक और कला एवं संगीत प्रेमी को खो दिया। डॉ. भाभा द्वारा प्रायोजित भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम आज भी देश के बहुआयामी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा रहा है।
-प्रदीप (pk110043@gmail.com)
from विज्ञान विश्व https://ift.tt/2AAkedc






0 comments:
Post a Comment